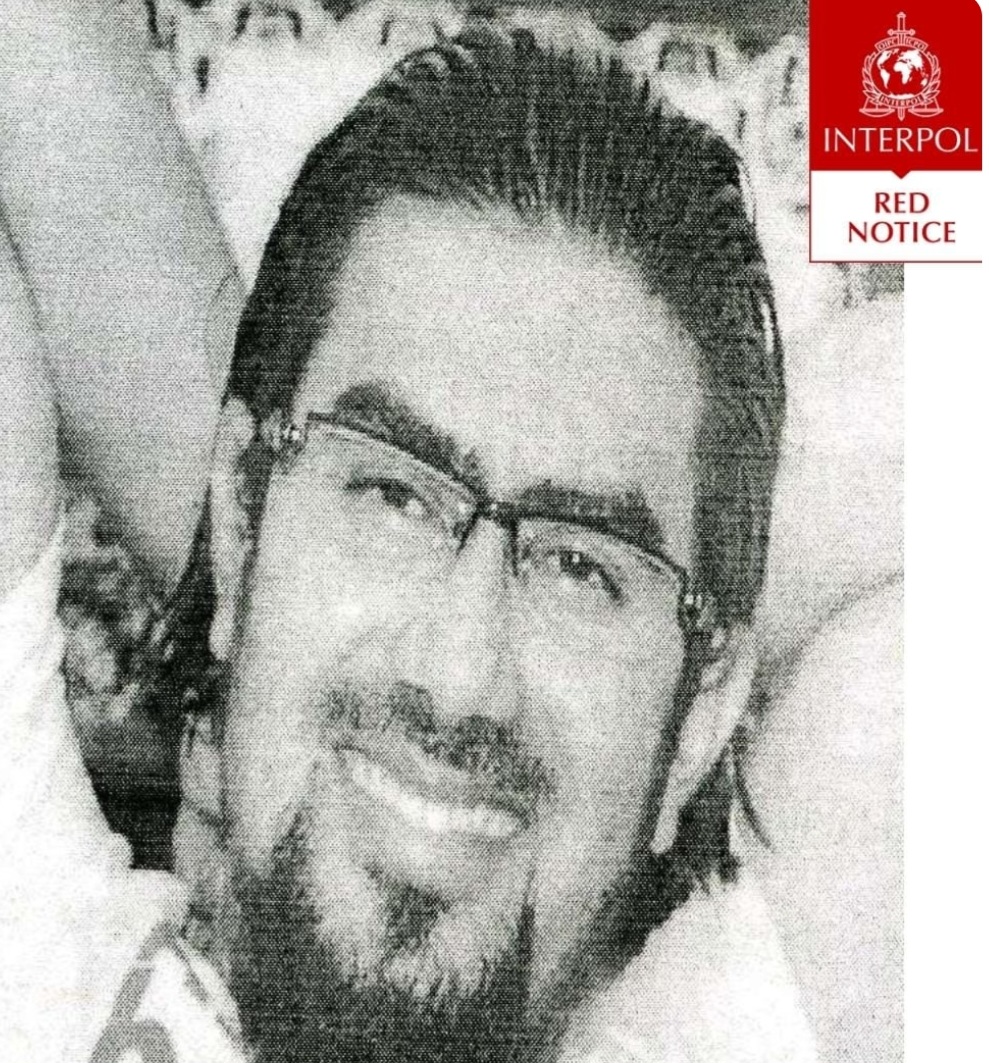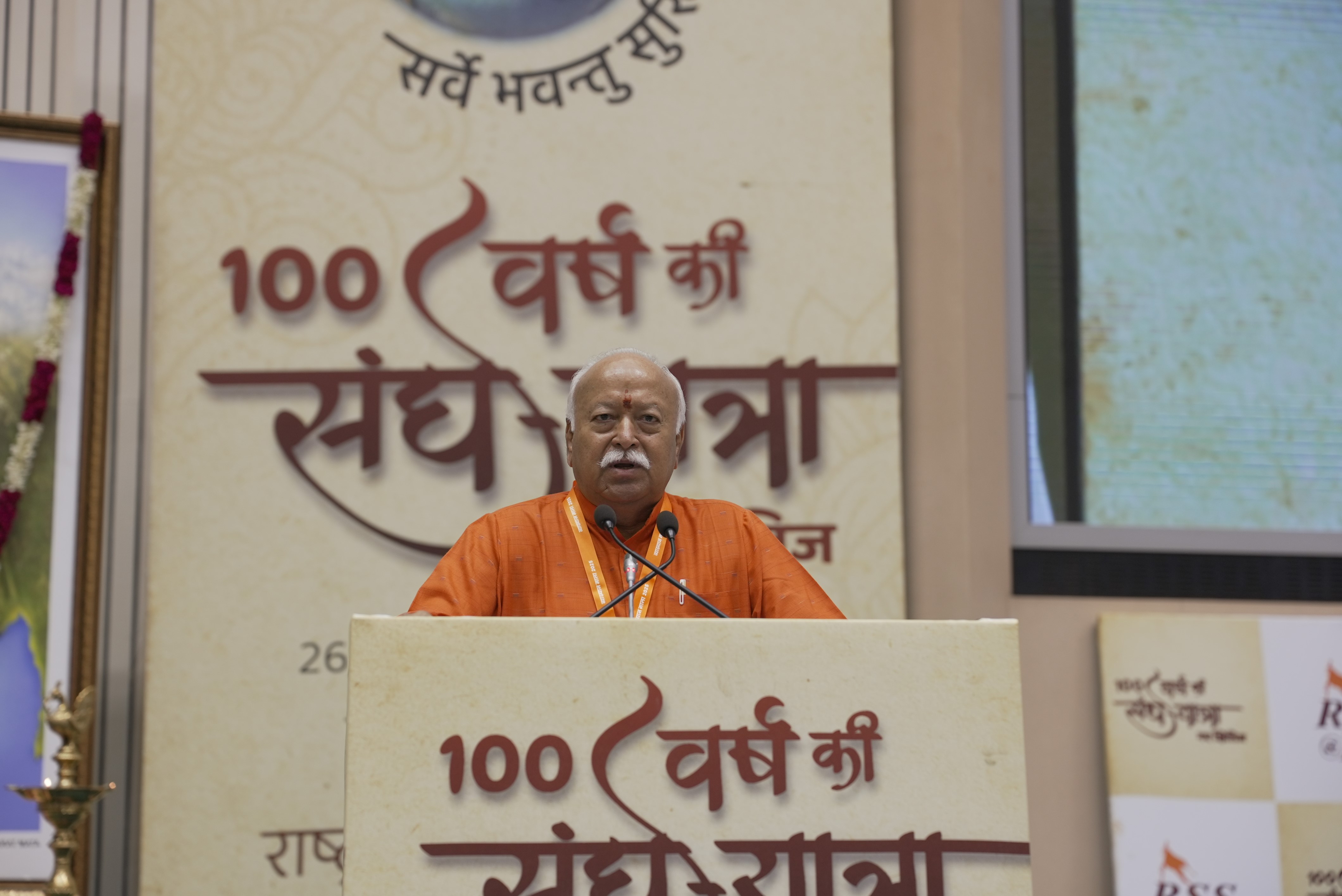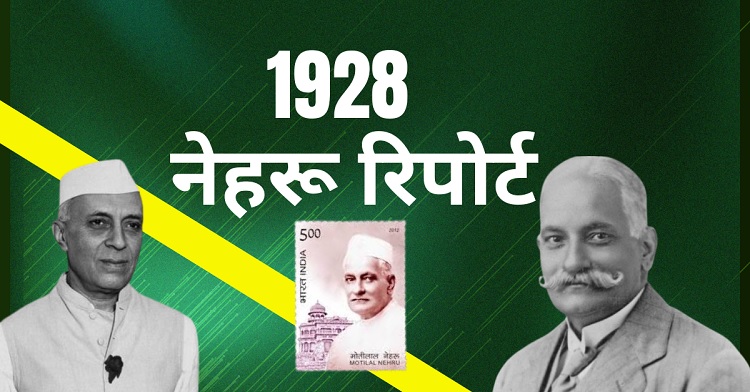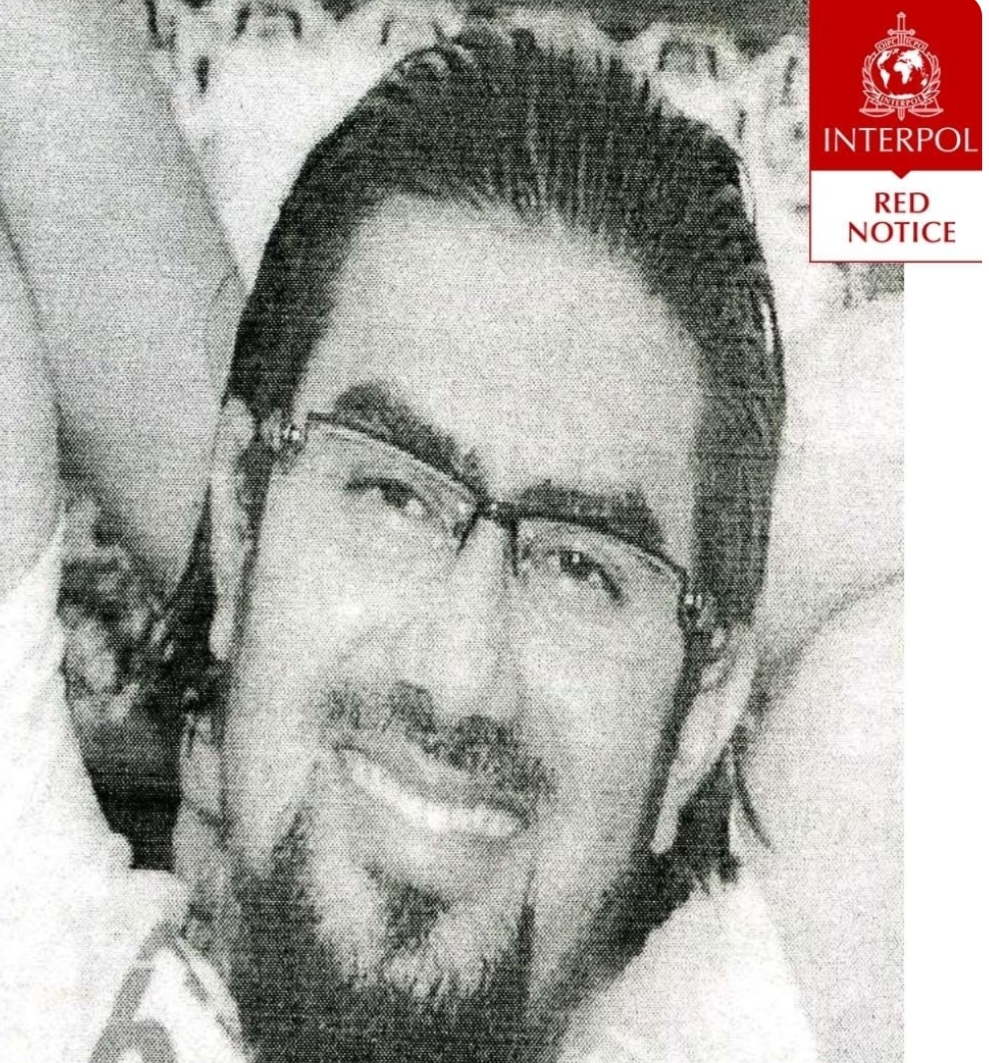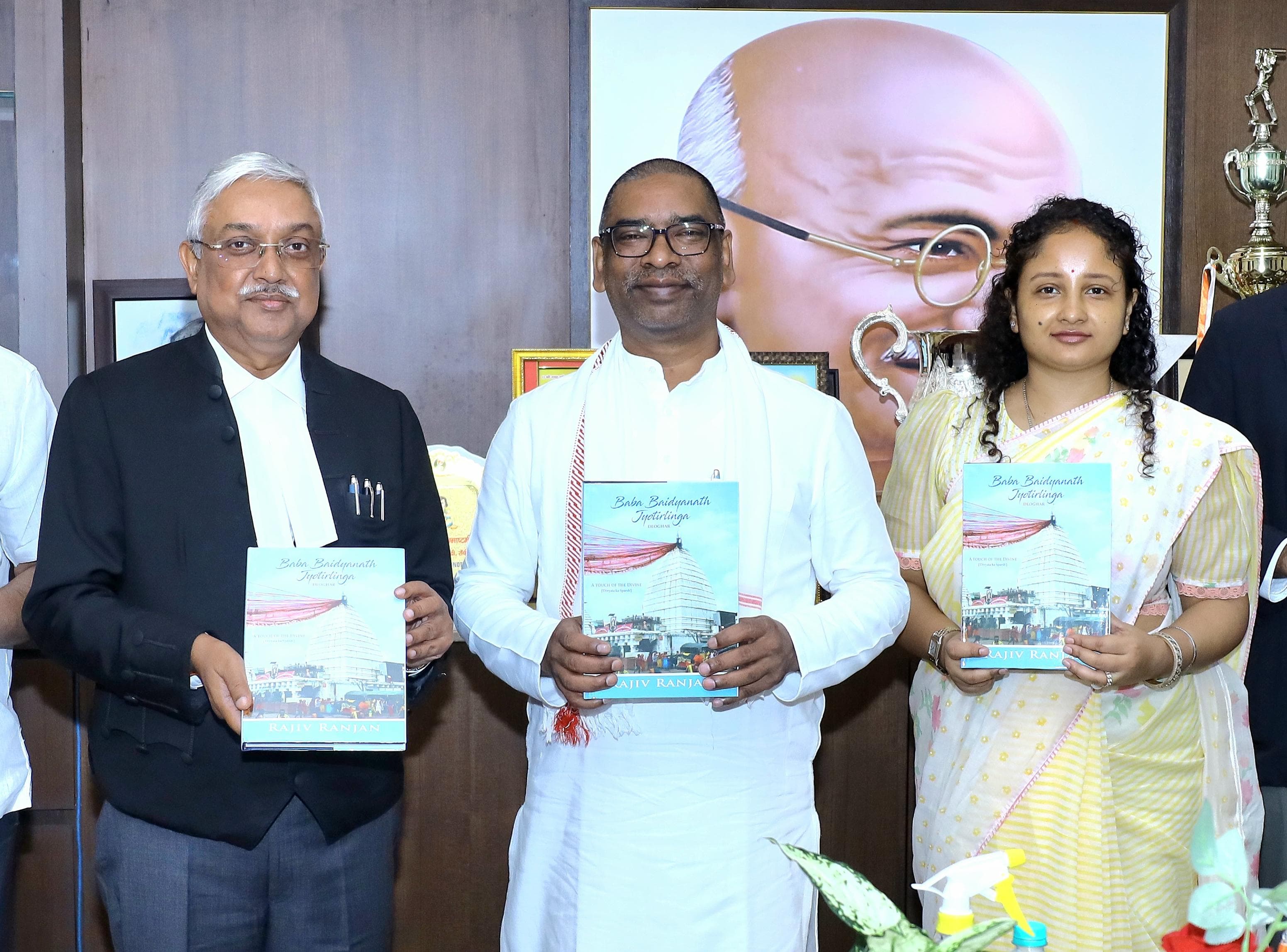“दण्ड और धर्म” के बीच संतुलन: 30 दिन की हिरासत और मंत्री पद विधेयक विवाद - डॉ. विश्वास चौहान
20 अगस्त 2025 को केंद्र सरकार ने संविधान (एक-सौ-तीसवाँ) संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया। प्रस्ताव यह है कि यदि कोई प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री/मंत्री लगातार 30 दिन तक ऐसे अपराध में न्यायिक हिरासत में रहे जिसका अधिकतम दण्ड 5 वर्ष या उससे अधिक हो, तो 31वें दिन उसका पद स्वतः समाप्त माना जाएगा।
भारतीय शासन–परंपरा में पद की पवित्रता (office of trust) का आग्रह अनादि काल से रहा है। यदि देखें तो महाभारत के शान्ति पर्व (राजधर्म) में भीष्म का उपदेश है कि राजा का महान धर्म दुरजन को दण्डित करना और सज्जनों की रक्षा करना है; मंत्रियों के दुराचार से कोश नष्ट हो तो गोपनीय रूप से सूचना लेने और दोषी को दण्डित करने का दायित्व राजा पर है। इसी प्रकार कौटिल्य अर्थशास्त्र में राजकोष अपहरण के चालीस प्रकारों एवम उपायों का विस्तार से उल्लेख है तथा भ्रष्ट अधिकारियों पर कठोर अनुशासन और पद से हटाने तक के उपाय सुझाए गए हैं,यह आज की जोखिम नियंत्रण, ऑडिट और “फ्रॉड डिटेक्शन” की आधुनिक भाषा में भी अनुकरणीय है।
प्रसिद्ध ग्रंथ मनुस्मृति , राजधर्म में “परीक्षित और शास्त्र–पारंगत मंत्रियों” की नियुक्ति और न्याय व्यवस्था में निष्पक्ष अन्वेषण व्यवस्था का निर्देश देती है ,अर्थात पद पर आचरण सर्वोपरि है, केवल पदवी नहीं। यह भारत की चिति का सामान्य चित्र था ।इन वाङ्मय संदर्भों का सार यह है कि शासन की प्रतिष्ठा व्यक्तिगत आचरण से जुड़ी है; यदि वह आचरण दण्डनीय संदेह के घेरे में दीर्घकाल तक हो, तो राज्यहित में पद से वियोजन न्यायसंगत माना गया है। भारत मे परकीय आक्रमणों और दासता से संघर्ष के दौर में नैतिकता के इन मानदंडों पर औपनिवेशिक छाया के बाद अमृतकाल के पंच परिवर्तन में इस छाया को हटाने के पंच प्रण को लेकर बीजेपी की वर्तमान सरकारें संकल्पित हैं।
संविधान सभा की बहसें: “पद की प्रसन्नता” और उत्तरदायित्व
अनुच्छेद 75(2), 164(1) और 239AA(5) के तहत मंत्री “ राष्ट्रपति या राज्यपाल के प्रासाद (प्लीजर) के सिद्धान्त” पर पद धारण करते हैं; छह माह में सदस्यता न बनने पर पद स्वतः समाप्त होता है। किन्तु हिरासत आधारित स्वतः पद त्याग का कोई सीधा प्रावधान नहीं है। प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 के तहत दोषसिद्धि (कम-से-कम 2 वर्ष की सजा) पर सांसद/विधायक तत्काल अयोग्य होते हैं, लिली थॉमस (2013) के केस में सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 8(4) को असंवैधानिक ठहराते हुए तुरंत जनप्रतिनिधियों की अयोग्यता को मान्य किया।
एक अन्य केस मनोज नारूला, 2014) के मामले में मंत्रियों की नियुक्ति/बर्खास्तगी पर न्यायालय ने कहा, "यह प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री का संवैधानिक विश्वास है; “मोरली टेंटेड” व्यक्तियों को मंत्री बनाना अवांछनीय है, पर विधायी व राजनीतिक उपचार अपेक्षित है । इसी प्रकार एक और केस बी.आर. कपूर बनाम तमिलनाडु (2001) के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा अपराध दोषसिद्ध और अयोग्य व्यक्ति का मुख्यमंत्री बनना/बने रहना अवैध इसलिए जेल या सजा से उपजी अयोग्यता के दौरान सीएम का पद पर बने रहना असंभव है। सुप्रीम कोर्ट ने Public Interest Foundation (2018) के केस में यहां तक कह दिया कि आरोप–पत्र भर से अयोग्यता नहीं; संसद से सख्त कानून बनाने का आह्वान।
न्यायालयीन कसौटी पर जब हम इस विधेयक को घिसते हैं तो अभी तक “हिरासत” (बिना दोषसिद्धि) से मंत्रीपद स्वतः नहीं जाता; यह संशोधन विधेयक यहीं परिवर्तन लाता है।
प्रस्तावित संशोधन: बदलाव क्या होंगे?
PIB/विधेयक–विवरण के अनुसार प्रस्तावित संशोधन से—
1. अनुच्छेद 75/164/239AA में नए उपबंध जोड़कर 30 दिन की सतत न्यायिक हिरासत (5 वर्ष या अधिक दण्डनीय अपराध) पर 31वें दिन पद का स्वतः–समापन होगा।
2. 30 दिन के भीतर जमानत मिलने पर पद सुरक्षित रहेगा; बाद में जमानत मिले तो पुनः पद संभालने की अनुमति का प्रावधान निहित है।
3. यह ढाँचा प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्रियों—और दिल्ली शासन (239AA) पर समान रूप से लागू होगा।
4. विधेयक संसदीय संयुक्त समिति को विचारार्थ भेजा गया है।
वैश्विक तुलनात्मक दृष्टि : दुनिया क्या करती है?
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखें तो ब्रिटेन में Representation of the People Act, 1981 में किसी सांसद को एक वर्ष से अधिक की सज़ा पर स्वतः अयोग्यता का उल्लेख है , साथ ही Recall of MPs Act, 2015 कुछ परिस्थितियों में मतदाता रिकॉल करा सकते हैं। अमेरिका में सांसद/मंत्रियों के लिए दोषसिद्धि पर भी स्वतः पद त्याग नहीं का कानून नही है पर सदन निष्कासन कर सकता है, पर स्वतः निष्कासन का अमेरिका में कोई संवैधानिक नियम नहीं है ।दक्षिण अफ्रीका में संविधान की धारा 47 में 12 माह से अधिक की सज़ा (बिना जुर्माना,विकल्प) पर विधायी अयोग्यता; हाल में वहां के चर्चित मामले जैकब ज़ुमा पर यह प्रावधान चर्चा में रहा। ऑस्ट्रेलिया में संविधान की धारा 44(ii) में एक वर्ष या अधिक की सजा योग्य अपराध में दोषसिद्ध और सज़ा के अधीन व्यक्ति सांसद बनने/बैठने से वंचित किया जाता है ।
अतः स्पष्ट है ,हिरासत आधारित स्वतः पद समाप्ति का 30 दिवसीय कठोर मानक भारत का विशिष्ट नवाचार है दुनिया के अन्य लोकतंत्रों में मानदंड दोषसिद्धि सज़ा की अवधि का है, हिरासत पर नहीं।
विधिक प्रभाव: न्याय, प्रशासन और राजनीति पर
1. नैतिक ,प्रशासनिक परिपाटी का संहिताकरण: जो बात अब तक शिष्टाचार और राजनीतिक दायित्व थी (tainted ministers न बनें), वह पहली बार संवैधानिक स्तर पर लिखित मानक बन जाएगी।
2. निष्पक्षता बनाम दुरुपयोग: जाँच एजेंसियों की कार्रवाई यदि निष्पक्ष हो तो यह प्रावधान शुचिता बढ़ाएगा; पर यदि अन्वेषण या हिरासत को हथियार बनाया गया, तो लोक इच्छा से निर्वाचित कार्यपालिका आकस्मिक अस्थिरता का शिकार हो सकती है, इसी आशंका पर विपक्ष ने इसे “असंवैधानिक/अलोकतांत्रिक” भी कहा है।
3. द्रुत न्याय की आवश्यकता: सर्वोच्च न्यायालय ने राजनीति के अपराधीकरण पर कई बार त्वरित निपटान/विधायी पहल का संकेत दिया है; यह संशोधन अंतरिम रोकथाम तो है, पर तेजी से मुकदमों का निस्तारण ही दीर्घकालीन समाधान होगा।
4. न्यायालयीन निर्णय सुसंगति:, लिली थॉमस ,बी.आर. कपूर मनोज नारूला केस में नैतिक मानक याद दिलाये गए हैं ।नया प्रावधान इन धारणाओं को हिरासत काल तक विस्तृत करता है, पर दोषसिद्धि के स्थान पर न्यायिक हिरासत को ट्रिगर बनाता है, यहीं न्याय सिद्धान्त की सूक्ष्म परीक्षा होगी।
क्या यह “भारतीय शास्त्र” की भावना से मेल खाता है?
भारतीय परंपरा में दण्ड (राज–शक्ति) का प्रयोजन धर्म का संरक्षण है, दमन नहीं। भीष्म की नीतियों से लेकर कौटिल्य तक का सूत्र यही है, “दुष्ट संयमन और हित संरक्षण।” यदि कोई मंत्री या अधिकारी लंबे समय तक ऐसी स्थिति में हो कि उस पर गंभीर अपराध का न्यायिक संदेह बना रहे, तो लोक विश्वास की रक्षा के लिए अस्थायी वियोजन (de-linking) राजधर्म सम्मत है। पर साथ ही न्याय–प्रक्रिया निष्पक्ष, त्वरित और दुरुपयोग रोधी हो, वरना दण्ड धर्म से विच्छिन्न हो जाएगा।
इस सम्पूर्ण विषय का एक ही सार है “यतो धर्मस् ततो जयः” , यह संशोधन शुचिता की कसौटी को संवैधानिक बना देता है; पर हिरासत और दोषसिद्धि के बीच की रेखा कानूनी ,नैतिक बहस भी माँगती है। 130वां संविधान संशोधन विधेयक भारतीय राजनीति में नैतिकता और जवाबदेही को सुदृढ़ करने का एक साहसिक प्रयास है। यह प्राचीन भारतीय मूल्यों, जैसे मनुस्मृति और महाभारत में वर्णित शासक की नैतिक जिम्मेदारी, को आधुनिक संदर्भ में लागू करने का प्रयास करता है।
संविधान सभा की बहसों से लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों तक, यह स्पष्ट है कि शासकों से उच्च नैतिक मानदंडों की अपेक्षा हमेशा रही है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी ऐसे प्रावधानों का चलन है, जो भारत के इस कदम को मजबूती प्रदान करते हैं।हालांकि, विपक्ष के विरोध को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह विधेयक संवैधानिक संतुलन और लोकतांत्रिक मूल्यों को प्रभावित कर सकता है, यदि इसे सावधानीपूर्वक लागू न किया जाए।
जेपीसी में होने वाली चर्चा इस विधेयक को और परिष्कृत कर सकती है, ताकि यह न केवल नैतिकता को बढ़ावा दे, बल्कि लोकतंत्र की नींव को भी मजबूत करे। इस प्रकार, यह विधेयक एक नये युग की शुरुआत का प्रतीक हो सकता है, जहां शासन की पवित्रता और जनता का विश्वास सर्वोपरि हो।यही भारतीय न्याय परंपरा का संतुलन है , दण्ड का प्रयोग तभी कि धर्म सुरक्षित रहे “यतो धर्मस् ततो जयः।”